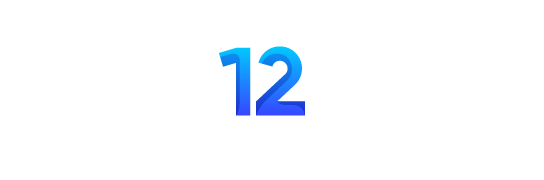भारत और चीन के बीच आर्थिक असमानता की जड़ें सिर्फ वर्तमान परिस्थितियों में नहीं, बल्कि इन देशों के ऐतिहासिक संदर्भ में भी गहरी निहित हैं। दोनों देशों ने पिछले शताब्दियों में अलग-अलग रास्तों का अनुसरण किया, जो आज के आर्थिक परिदृश्य को आकार देते हैं। इन ऐतिहासिक कारणों को समझने से हमें यह भी समझ में आता है कि आज जो अंतर दिखता है, वह कैसे विकसित हुआ।
ऐतिहासिक संदर्भ: ब्रिटिश उपनिवेशवाद और मिंग साम्राज्य
चीन और भारत के ऐतिहासिक विकास में दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो उनके आज के आर्थिक परिदृश्य को प्रभावित करते हैं।
- ब्रिटिश उपनिवेशवाद (भारत) भारत ने 200 साल तक ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन किया। ब्रिटिश शासकों ने भारतीय संसाधनों का शोषण किया और औद्योगिकीकरण को न दबाया, बल्कि कृषि पर जोर दिया, जिससे भारत की औद्योगिक विकास की क्षमता रुक गई। इसके परिणामस्वरूप, भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ गई और उपनिवेशीकरण के बाद भी आर्थिक ढांचा कमजोर रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, भारत ने आत्मनिर्भरता की नीति अपनाई, लेकिन वह बहुत धीमी गति से विकसित हुआ, क्योंकि उसकी औद्योगिक और बुनियादी ढांचा संबंधी योजनाएँ प्रभावी नहीं हो सकी थीं।
- मिंग साम्राज्य और क्विंग साम्राज्य (चीन) दूसरी ओर, चीन में मिंग और क्विंग साम्राज्यों का इतिहास था, जिन्होंने लंबे समय तक कृषि और व्यापार में सुधार किए। हालांकि, चीन में 19वीं शताब्दी के मध्य में औपियम युद्धों के बाद ब्रिटिश और अन्य पश्चिमी शक्तियों के प्रभाव का सामना करना पड़ा, लेकिन 1949 में माओ जेडॉन्ग द्वारा चीनी क्रांति के बाद चीन ने सशक्त रूप से अपना साम्राज्यिक और आर्थिक ढांचा फिर से खड़ा किया। माओ के बाद, 1978 में जब डेंग शियाओपिंग ने चीन में आर्थिक सुधार शुरू किए, तो चीन ने धीरे-धीरे एक नया औद्योगिक और वैश्विक व्यापारी केंद्र बनने की दिशा में कदम बढ़ाया।
1. 1980 के दशक में प्रारंभिक सुधार और दिशा का निर्धारण
भारत और चीन दोनों ने 1980 के दशक में अपनी-अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार शुरू किया। हालांकि, चीन ने अपने सुधारों को तेज़ी से और केंद्रीकृत रूप से लागू किया, जबकि भारत ने धीरे-धीरे इसे अपनाया।
- चीन के सुधार: 1978 में डेंग शियाओपिंग के नेतृत्व में चीन ने “खुलापन और सुधार” की नीति अपनाई। चीन ने विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए आर्थिक विशेष क्षेत्रों (SEZs) की स्थापना की, और उत्पादन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को मजबूत किया। चीन ने जल्दी ही अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाया और दुनिया के “फैक्ट्री” के रूप में उभरा। इसके साथ ही, चीन ने कृषि से उद्योग की ओर बड़े पैमाने पर पलायन किया, जिससे औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिला।
- भारत के सुधार: भारत ने 1991 में आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन चीन से काफ़ी देर से। भारत ने खुद को विदेशी निवेश के लिए खोलने और व्यापार की नीतियों में लचीलापन लाने का प्रयास किया। हालांकि, भारत का औद्योगिकीकरण अपेक्षाकृत धीमा था, और उसने कृषि के क्षेत्र को प्राथमिकता दी, जो कि चीन के तेज़ औद्योगिकीकरण के मुकाबले काफी पीछे था।
2. निवेश की कमी और संरचनात्मक समस्याएं
भारत में हमेशा से निवेश की कमी रही है। चीन ने जहां अपनी अर्थव्यवस्था को विकासशील देशों से अलग बनाने के लिए विदेशी निवेश और बुनियादी ढांचे में भारी निवेश किया, वहीं भारत में बड़े पैमाने पर निवेश की कमी और सरकारी नीतियों की जटिलता विकास को बाधित करती रही है। उदाहरण के लिए, भारत के निर्माण क्षेत्र में काफी निवेश की आवश्यकता थी, लेकिन इसमें सुधार की गति बहुत धीमी रही।
चीन ने तेजी से औद्योगिकीकरण और उत्पादन क्षमता को बढ़ाया, जबकि भारत में इससे उलट, सेवाओं और कृषि क्षेत्र पर ज्यादा जोर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप, चीन ने निर्यात बढ़ाया और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया, जबकि भारत का निर्यात कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सका।
3. शैक्षिक और सामाजिक सुधारों में भिन्नताएँ
चीन ने अपनी शिक्षा प्रणाली पर बड़ा ध्यान दिया, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी और विज्ञान में, जबकि भारत में कई दशकों तक प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में धीमी प्रगति रही। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में समानता की कमी रही, जिससे बहुत से गरीब वर्ग के बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित रहे। दूसरी ओर, चीन ने बहुत जल्दी और प्रभावी ढंग से अपनी शिक्षा प्रणाली को मजबूत किया, जिससे वहां की कार्यबल की गुणवत्ता में सुधार हुआ।
4. लोकतांत्रिक संरचना बनाम केंद्रीकृत शासन
भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होने के कारण नीतियों को लागू करने में कभी-कभी जटिलताएँ होती हैं, क्योंकि विभिन्न राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों के बीच समझौतों की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत, चीन का केंद्रीकृत शासन निर्णय लेने और नीतियों को जल्दी लागू करने में सक्षम है, जिससे वहां के प्रशासन में तेज़ी आई। इस प्रणाली के कारण चीन ने आर्थिक सुधारों को तीव्रता से लागू किया, जबकि भारत को हर कदम पर संघर्ष करना पड़ा।
निष्कर्ष
भारत और चीन के आर्थिक अंतर की गहरी जड़ें ऐतिहासिक और संरचनात्मक हैं। चीन ने जल्दी औद्योगिकीकरण, शिक्षा, और नीतिगत सुधारों के जरिए तेजी से विकास किया, जबकि भारत ने अपनी धीमी और धीरे-धीरे चलने वाली नीति के कारण पिछड़ता गया। हालांकि, भारत में अब भी विकास की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन उसे इन ऐतिहासिक कारणों और मौजूदा संरचनाओं से निपटने के लिए रणनीतिक बदलावों की आवश्यकता होगी।